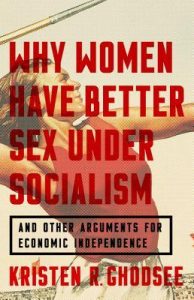[मूल कहानी- शहीद कामरेड रेणुका, अनुवाद- असीम सत्यदेव]
भरपूर मुस्कराते हुए सोनू हर डग भर कर चल रहा था। उसने अभी-अभी चलना सीखा था। सारा दिन सोने और उठने पर दूध पीने से शायद माँ के प्यार से उसका दिल संतुष्टि से भर गया था और उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति और खुशी झलक रही थी। शाम को सूरज की रौशनी में उसका काला बदन चमक रहा था। पूरे विश्वास के साथ हर डग भरते हुए कुछ पकड़ने के लिए उसने एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके लिए उसके हर कदम एक बड़ी जीत थी। उस जीत के गर्व से उसकी आँखों, चमक खींची। उसको देखकर शायद ही कोई हो जिसे प्यार नहीं उमड़ता हो।
अपने आंगन में खटिया पर बैठे हुए बोकलू ने सोनू को अपनी ओर आते देख अपने हाथ फैला दिये। बोकलू को हाथ फैलाते देख सोनू ने चुलबुली हँसी के साथ चाल तेज कर दी। बोकलू खटिया पर बैठा नहीं रह सका। खटिया से वह बॉह फैलाये हुए उठा। आंगन में दो कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल वह दोनेां हाथों से उस छोटे बच्चे को उठाकर उसके गाल चूमता और कसकर गले से लगा लेता कि उसी पल सोनू की माँ गुलारी तेजी से आयी और उसने सोनू को उठा लिया और फिर बोकलू से गुस्से में बोली, ‘‘अपने गन्दे हाथों से इसे कभी छूना नहीं।’’ इतना कहकर वह जल्दी से तेज कदमों से अपने घर लौट गयी। अपनी आजादी छिन जाने और जबरदस्ती उठा लिये जाने से सोनू रोने लगा। बाकलू भौचक रह गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। आंगन के पीछे बरामदे में अपने घर से उसी समय आयी बोकलू की पत्नी कन्नी तथा वहीं दूसरी खटिया पर बैठी बोकलू की माँ एडिमी ने यह सब देख लिया।
गुस्से में कन्नी ने कहा, यह गुलारी हमेशा से ऐसी ही है। इन्हें देखते ही उसकी आँखें गुस्से से जलने लगती है है। ‘‘चुप रहो उसने सुन लिया तो और ज्यादा लड़ाई होगी।’’ एडिमी ने कहा।
लड़ाई के डर से हम कब तक चुप बैठे रहेंगे ? वह जो चाहे सो करती रहे क्या हमें बर्दाश्त करते रहना चाहिए ?’’….. कन्नी की आवाज में गुस्सा और दर्द मिले हुए थे।
‘‘हमें चुप बैठना चाहिए। अपनी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना ही चाहिए। कम से कम इस तरह यहाँ रहने देने के लिए हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए।’’ एडिमी ने कहा। कन्नी का गुस्सा शांत होने लगा। उसने अपनी गलती मान ली। ऐसे में बड़ी पंचायत (गाँव की आम सभा की बैठक में) में वहाँ उसे माफ कर देने का फैसला लेकर उन्होंने इसे अपने में से ही एक मान लिया था। यहाँ तक कि पार्टी के लोग भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे।’’ वह बोली। ‘‘यह सही है कि उन्होंने कहा था कि हर किसी को उसे अपना लेना चाहिए…. लेकिन क्या कहने भर से जल्द से जल्द हर कोई सब कुछ भूलकर इन्हें अपना सकता है। बेचारा बच्चा, कितना कुछ उसने झेला है।
बोकलू फिर से खाट पर लेट गया और अपनी आँखें मूँद ली। उसके कानों में अपनी पत्नी और माँ की बातचीत पहुँच रही थी। उसकी यह हालत में देख दोनों औरतों के दिल दुःख से भर गये थे।
उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा ‘‘उदास मत हो मेरे बेटे। हमें ये सब कुछ दिन और सहना है। समय बीतने के साथ हर कोई भूल जायेगा।
वहाँ से उठकर कन्नी घर के कामों में लग गयी। एक महीने पहले पंचायत में गुलारी के कहे गये कटु वचन उसके कानों में आज भी गूँज रहे थे ।
’ ’ ’ ’
क्या !! क्या हमें इन लोगों को जिन्दा छोड़ देना चाहिए ? ये वही है जो झुंड में गुण्डों को अपने साथ यहाँ लाये हैं इनके बिना झुंड के लोग हमारे गाँव पर इतनी मुसीबत नहीं ला सकते थे। पोजल ने गुस्से से उबल कर कहा।
‘‘यह सही है लेकिन अब उन्होंने अपनी गलती मान ली है…’ जनताना सरकार के अध्यक्ष एडामल ने यह कहते हुए आगे कहना शुरू किया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दुलारी ने बीच में दखल देते हुए कहा ‘‘क्या मतलब है आपका ? ये सब करने के बाद क्या अपनी गलती मान लेना काफी है ? क्या हम उन्हें छोड़ दें ? हम अगर इनके टुकड़े-टुकड़े कर दें तब भी यह पाप नहीं है।
हाँ, इन्हें जिन्दा नहीं छोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर इन्हें मार डालना चाहिए कमली ने कहा। हाँ। ‘‘इन्हें मार डालना ही चाहिए।’’ कई लोगों की आवाजों गूँजने लगी। हर कोई गुस्से से उबल रहा था।
यह घटना दण्डाकारण्य के बैरामगढ़ क्षेत्र के पौटम गाँव की है। इस गाँव में लगभग 150 घर हैं। गाँव के निवासियों के अलावा अन्य चार गाँवों के लगभग पाँच-छः सौ लोग गाँव के दक्षिणी तरफ के आम के पेड़ांे के पास जनताना सरकार के तहत आये थे। अगस्त के पहले महीने के चलते आकाश में बादल थे। दोपहर का खाना खाने के बाद पंचायत में हर कोई आया था। पंचायत का संचालन जनताना सरकार के कानूनी विभाग की इंचार्ज जैनी कर रही थी।
लोग आधा गोलाकार स्थिति में बैठे थे। कुछ लोग छोटे पत्थरों और कुछ लोग लकड़ी के लट्ठों पर बैठे थे। कुछ लोग जमीन पर जूते निकलाकर उसी पर बैठ गये थे। कुछ लोग खड़़े थे। उनके सामने सिर झुकाकर बोकलू और मंगल बैठे थे। उनके दाहिनी ओर गुरिल्ला स्क्वाड के सदस्यों के साथ एडामल तथा जनताना सरकार के कुछ अन्य सदस्य बैठे थे। बायीं तरफ बोकलू और मंगल के परिवार के सदस्य थे। जैनी खड़ी थी।
‘‘यह सही है कि इन्होंने भयानक गलतियाँ की। लेकिन ये गलतियाँ खद इनकी पहल पर नहीं हुई। सरकार की योजना के तहत उकसे एक हिस्से के रूप में झुंड लायी जुडुम नेताओं और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ये गलतियाँ करने के लिए मजबूर किया। आगे एडामल ने विस्तार से इस बारे में बताना शुरू किया तो गुस्से से सोमल ने दखलन्दाजी करते हुए कहा – उस समय उनकी अक्ल को क्या हो गया था ? पहली बात उन्होंने क्यों जुडुम में शामिल होना तय किया। वे हमारे निर्देशों के खिलाफ गये और अब उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें अपने चेहरे दिखाने की ?
‘‘गैर जानकारी में या डर की वजह से कई लोग जुडुम में शामिल हो गये। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे वापस आ रहे हैं। जिन्होंने अपनी गलतियाँ मान ली है हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए? जनताना सरकार का सदस्य जुगरू बोला।
‘‘कैसी गैर जानकारी ? क्या आप सबने पहले से एक मीटिंग में कमेटी की तरफ इन्हें बताया नहीं था ? गुलारी ने प्रतिवाद किया।
हालाँकि हमने उन्हें बताया था लेकिन उस समय हालात क्या थे ? दुश्मन भी बड़े पैमाने पर प्रचार में लगा था, कई लोगों ने उस प्रचार पर यकीन कर लिया था। जुनरू ने समझाया।
वे खाली जुडुम में शामिल ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने स्पेशल पुलिस आफिसर (एस0पी0ओ0) बनने का फैसला लिया। कितनी बार हमारे गाँव पर धावा मारा ? कितने घरों को उन्होंने जलाया ? कितनी फसल उन्होंने जलायी ? कितनों को उन्होंने मार डाला ? कितनी औरतों से उन्होंने बलात्कार किया सोमवती का गुस्सा चरम पर था?
उन्होंने हमारे गाँव के पाँच लोगों की जान ली। पाँच औरतों से बलात्कार किया।’’ …. एडिमी ने जोड़ा।
एडिमी के मुँह से जैसे ही यह वाक्य निकला, गुस्से और दुःख का भाव गुलारी, कामिल और एथी में आ गया। ये तीनों बलात्कार की शिकार थी। दो अन्य जवान औरतें गाँव छोड़ चुकी थी और कटु अनुभव से बचने के लिए दूर गाँवों में रिश्तेदारों के पास रह रही थी।
सलवा जुडुम हमले से हमारे गाँव को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लेकिन हम जानते है कि इन दोनों ने व्यक्तिगत रूप से कोई हत्या या बलात्कार नहीं किया।’’ एडामल ने कहा व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया हो लेकिन जिस भीड़ को ये लाये थे सब कुछ उसी ने किया। सोमदारी ने कहा।
लोगों की दलीलें और उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनने-समझने के लिए जैनी आगे-पीछे घूमती रही। उसने खुद दृढ़ता से महसूस किया कि अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी खुद की राय जो लोग जाहिर कर रहे थे और बहस कर रहे थे वह उनमें शामिल होना चाहती थी। लेकिन कानूनी विभाग की जिम्मेदारी होने के कारण वह जानती थी कि वह मंच उसकी खुद की दलीलों का नहीं है इसलिए उसने बलात खुद को काबू में रखा।
जब कमेटी सदस्यों की कोशिशों के बावजूद लोग सहमत नहीं हो पा रहे तो स्क्वाड का कमांडर मंगतू खुद उठ खड़ा हुआ। उसने सहमति के तरीके से बोलना शुरू किया, कामरेड मुझे जो सोचना और कहना है उसे सुनिये। जब सलमा जुडुम शुरू हुआ तो लोगों में चिन्ता और डर था जब यह प्रचार किया गया कि यहाँ से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जायेगा और आज नहीं तो कल हर किसी को पुनर्वास शिविर में रहना होगा, तब यह डर ज्यादा बढ़ गया। इस प्रचार के बावजूद कई लोग हिम्मत के साथ खड़े हो गये। उनका मानना था कि यदि यह जमीन छोड़ दी तो उनका कोई जीवन नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ डटे रहने का फैसला लिया जो हो गया। लेकिन कुछ लोग डटे हुए थे। कुछ असमंजस में थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ डटे रहने पर वे बेकार में मार डाले जायेंगे। उन्होंने विश्वास कर लिया कि पार्टी का यहाँ से सफाया हो जायेगा या यहाँ से पीछे हट जायेंगी। इसलिए वे जुडुम में शामिल हो गये।
एक बार जुडुम में शामिल हो जाने पर उनको कोई आजादी नहीं थी। उनको स्पेशल पुलिस आफिसर में शामिल होने को कहा जाता तो उन्हें शामिल होना पड़ता। यदि गुण्डों के दल में शामिल होने को कहा जाता तो उन्हें शामिल होना पड़ता। हो सकता है कुछ लोग अपनी मर्जी से शामिल हो गये हो लेकिन कुछ तो दबाव में मजबूरन शामिल हो गये थे। लेकिन उनको जैसा डर था वैसे पार्टी का सफाया नहीं हुआ। हमारा प्रतिरोध बढ़ा। इसके अलावा हमने जुडुम में शामिल लोगों से अपने गाँव वापस आने का आह्वान किया। इसके अलावा से शिविरों में हो रहे अत्याचार सहन नहीं कर सके। वहाँ बर्बाद हो रही जिन्दगी से वे तंग आ गये। इसलिये बहुत लोगों ने सही दिशा में सोचना शुरू कर दिया और वे पी0एल0जी0ए0 (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की सुरक्षा में वापस गाँव आकर रहना चाहते थे। यह एक अच्छा विकास है। हालाँकि शुरू में उन्होंने गलतियाँ की, वे उसे सुधारने के लिए तैयार है ? यह हमारी पार्टी और हमारे संघर्ष के प्रति बढ़ते विश्वास का सूचक है। तो हमें ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए या दूर कर देना चाहिए ? जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं उन्हें दूर हटा देने से क्या हमारे आन्दोलन को नुकसान नहीं पहुँचेगा? क्या इससे जुडुम की ताकत नहीं बढ़ेगी ?
फिर भी हम यह नहीं कह रहे कि जो जुडुम में शामिल हुए और प्रचंड हत्याओं तथा बलात्कार किये या क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया उनको माफ कर देना चाहिए। बोकलू और मंगल एस0पी0ओ0 में शामिल हुए, यह सच है। तीन महीनों तक उन्होंने काम किया। हमारे गाँव में जुडुम को लेकर आये। उस दौरान जुडुमजनों ने यहाँ अत्याचार और हत्यायें की ? तथापि इन्होंने खुद ये काम नहीं किये। यहाँ तक शिविरों में भी उन्होनंे लोगों को पीटा लेकिन इन्होंने चरम क्रूरता नहीं की और यहाँ तक हमारी रिपोर्ट का संकेत है कि इन्होंने कोई हत्या या बलात्कार नहीं किया। उन्होंने हमारा आह्वान सुना और वापस आ गये। इसके अलावा जब वे जुडुम में शामिल हुए थे तब उनके परिवार हमारे बीच ही रहे थे। यहाँ तक कि जनसंगठनों में जब इन्होंने काम किया तो उनका व्यवहार अच्छा था। किसी ने भी इनके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। अपनी गलतियाँ इन्होंने मान ली। इसलिए पार्टी और जनताना सरकार दोनों का विश्वास है कि इन्हें माफ कर देना और छोड़ देना अच्छा होगा। इस पर विचार कीजिए: यदि जो हमारे आह्वान पर विश्वास करके वापस आ गये यदि हम उन्हें मार डाले तो क्या कोई और शिवरों को छोड़कर आने की इच्छा करेगा ? अपने दिमाग में सावधानी से हमारी राय रखिये औरहमें अपना फैसला बताइये।
हम किसी पर सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए मगतू ने यह बात समाप्त की।
मंगतू के शब्दों ने कुछ प्रभाव डाला। उनके गुस्से की जगह विचार करने, फिर भी गुलारी समेत कई लोग सहमत नहीं हुए।
मंगतू दादा आप इस तरह ही बोलेंगे। उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने हमें मारा-पीटा और हम पर हमला किया।’’ उसने कहा और उसकी आवाज में दुःख, गुस्सा और नाराजगी धुली-मिली थी।
मंगतू ने उसकी ओर इस तरह से देखा जैसे वो घायल हो गया हो और जवाब में वो कुछ नहीं बोल सका।
‘‘इतना गलत मत बोलो गुलारी। क्या हमारा दर्द पार्टी का दर्द नहीं है ? यदि हमारे लिए नहीं है तो फिर पार्टी किसके लिए है ? एडामल ने कहा उसके शब्दों ने मंगतू दादा को कितनी चोट पहुँचायी है इसका एहसास होते ही गुलारी ने अपने कठोर शब्दों के प्रति अफसोस जाहिर किया। फिर भी बोकलू और मंगल को सजा देने पर वह अपने दृढ़ निश्चय पर कायम रही। वह कैसे भूल सकती थी कि दो महीने पहले वोकलू और मंगल द्वारा लाये गये जुडुम लोगों ने उसके हाथों से उसका बच्चा छीन लिया और उस पर हमला बोल दिया था ? अपने असहाय बच्चे का रोना और खुद अपने संघर्ष को याद अब भी ताजे जख्म की तरह थी।
‘‘यदि वे एस0पी0ओ0 में शामिल करते हुए कर डर हुए तब भी यदि उनका व्यवहार सामान्य होता तो अच्छा रहता। लेकिन वे उस क्रूर और दुष्ट कैरी उंगल के नजदीकी थे। यदि वे उसके करीबी दोस्त थे तो कौन जानता है कितने बुरे काम वे कर चुके है। गंगल ने कहा।
कैरी उंगल का नाम आते ही गुलारी और कई अन्य लोगों के लिए घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसका पशुवत व्यवहार और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने का तरीके ने गुलारी को एक बार फिर से नफरत से भर दिया।
कैरी उंगल एक निर्दयी जमींदार था। लेकिन आन्दोलन ने उसे काफी कमजोर कर दिया था। वह निर्दयी आदमी पलट वार करने के मौके इंतजार में था। अब जुडुम को साथ वह फिर से उठ खड़ा हो गया, पोट्टम से चार किलो मीटर की दूरी पर जांगला में शरणार्थी शिविर में रहता था। गाँवों के घावों में उसने सक्रिय भागीदारी की और कुख्यात सलवा जुडुम नेता के रूप में साख अर्जित की।
‘‘आप क्या कहते है मंगतू दादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हें रहने नहीं दे सकते। गुलारी के स्वर में दृढ़ता थी और कई लोगों में उसकी भावना का स्वर गूँजे।
जैनी को पहले डर सता रहा था कि मंगतू के स्वर में हर कोई बह जायेगा और उन्हें बगैर सजा के जान देने की सलाह दे सकता है। उसे औरों को सुनकर राहत महसूस हुई। वो अपनी खुशी छिपा नहीं सकी।
कॉमरेड मैं आपका गुस्सा समझता हूँ। जो तकलीफ आपने गुजारी है उसके बाद इस तरह महसूस करना स्वाभाविक है लेकिन हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। हमें इस बारे में पार्टी के रवैये को ध्यान में रखने और उसे आगे ले जाने की जरूरत है। पार्टी की इस बारे में स्थिति यह है कि जुल्म के नेताओं को मार डालना और जुल्म शिवरों से वापस आने वाले को माफ कर देना तथा उन स्पेशल पुलिस अफसरों को भी माफ कर देना है जिन्होंने क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया है और अपनी ओर से समर्पण कर देते है। हमारी पार्टी की रणनीति उन्हें अपनी कतारों में समाहित करने और राजनीतिक रूप से विकसित करने में सहायता करने की है। ऐसे लोगों ने गाइड के रूप में काम किया, घर जलाए, लोगों को पीटा लेकिन उन्होंने किसी की हत्या या बलात्कार नहीं किया। वे कैरी उंगल के करीबी थे लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि उसके द्वारा उन्हें जान से मार डालने के डर ने उनसे ऐसा कराया। अब यदि हम उन्हें मार डालते है तो यह हमारी पार्टी की नीतियों के खिलाफ होगा।’’ मंगतू ने समझाया।
‘‘कौन जानता है कि वे सही में बदल गये है या फिर किसी चाल के तहत कैरी उंगल ने उन्हें यहाँ भेजा है।’’ कामली ने सन्देह व्यक्त किया। हो सकता है कि वे सिर्फ समर्पण का नाटक कर रहे हैं। ऐथी ने अपनी तरफ से जोड़ा। ‘‘यदि कोई कपट पूर्ण इरादा उनका है तो हम उन पर नजर रख सकते है। कमेटी, मिलीशिया और लोगों की नजर उनके हर कदम पर होगी। हम उन्हें पूरी आजादी नहीं देंगे। हम कुछ शर्ते लागू करेंगे जैसे बाहरी व्यक्ति से बात न करना या गाँव छोड़कर नहीं जाना।’’ मंगतू ने बात आगे बढ़ाई। एक व्यक्ति ने सहमति में कहा – ‘‘हाँ शर्तें रखना एक अच्छा विचार है और बाकी लोगों के स्वर भी गूँजे हाँ, हाँ।’’
‘‘ये ठीक है कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की ओर लोगों को पीटा है और घर जलाए है। तो क्या इसके लिए उन्हें कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए।’’ एक व्यक्ति ने पूछा और उससे सहमत हुए लोगों ने कहा – ‘‘हाँ, हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते।’’
जल्द ही उस जगह में शोर-गुल उठने लगा। विभिन्न आवाजें एक दूसरे के ऊपर आने लगी और यह समझ में आना मुश्किल हो गया कि कोई क्या कह रहा है।
जैनी को अपनी जिम्मेदारी याद आई। ‘‘कॉमरेड शोर न मचाइये। एक-एक कर के बोलें।’’ दो-तीन बार उसने चिल्लाकर कहा और धीरे-धीरे शोर बन्द हो गया।
यदि उन्हें मार डालना नहीं है तो उन्हें कुछ सजा देनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा और कई अन्य स्वर गूँजे ‘‘हाँ यह होना चाहिए।’’
जैनी ने गौर से देखा कि भीड़ पर मंगतू दादा के शब्दों ने अच्छा प्रभाव डाला है जो पहले उन्हें मार डालने को तत्पर थे वे जब उसके विकल्प पर विचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे थोड़ी निराशा करते हुए उसने पूछा-‘‘हमें उन्हें क्या सजा देनी चाहिए ? उन्हें मारे और फिर जाने दें। लेकिन गुलारी और उसके समर्थकों ने जोर दिया – नहीं हमें उन्हें मार ही डालना चाहिए।’’
जैनी की चिन्ता दूर हो गयी और वातावरण फिर शोर-गुल वाला हो गया। वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ समय तक वो चिल्लाई फिर उसने पंचायत आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो एक किनारे हो गयी। कमेटी के अन्य सदस्यों को बुलाया और उनसे राय मशवरा लिया। वो भीड़ की तरफ उन्हें संबोधित करने आई।
पंचायत शुरू होने के समय से ही बोकलू और मंगल सिर झुकाये बैठे थे। वे एक किस्म की उदासीनता के घेरे में थे। उनके परिवार के लोगों की दशा दयनीय लग रही थी जैसे वे चुपचाप दया की याचना कर रहे हों। बोकलू और मंगल खुद अपनी किस्मत से बेखबर लग रहे थे।
जैनी ने लोगों की तरफ नजर घुमाते हुए कहा ठीक है कॉमरेड, हर कोई मामले को अच्छी तरह समझ चुका है। आपने सारी दलीलें सुनी। अब बहुमत के अधार पर हमें फैसला लेना है। कुछ की राय है उन्हें पीटा जाये और छोड़ दें। इसलिए जो इन्हें मौत की सजा देने के पक्ष में है वे हाथ उठायें।
बोकलू और मंगल के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। यह जानते हुए भी कि हाथ उठाये जाने के आधार पर उनकी जिन्दगी या मौत का फैसला होगा वे उदासीन बने रहे मानो अपनी किस्मत से बेखबर हो गये हों। फिर भी उनके पारिवारिक सदस्यों के चेहरों पर डर फैल गया और अनुमान लगाने में साँसें थम गयीं।
हवा में कई हाथ उठ गये। जैनी ने गिनती शुरू की। बोकलू और मंगल ने अब भी सिर नहीं उठाया लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के चेहरें चिन्ता से भर गये थे जब उन्होंने उठे हाथों की तरफ घूर कर देखा। ये केवल उठे हुए हाथ नहीं बल्कि बोकलू और मंगल की गर्दनों पर वार करने वाली तलवारे लग रहे थे।
गिनती करने के बाद जैनी ने कहा, अब जो यह सोचते हैं कि इन्हें पीट कर छोड़ दिया जाये अपने हाथ उठायें। यह एहसास करने पर कि मौत की सजा से से सहमत उठाये हाथों की संख्या कम है, उसे बेचैनी हो गयी थी।
अब जो सोचते है कि न तो इन्हें पीटा जाये और न ही मौत की सजा दी जाये, वे हाथ उठायें। वह महसूस कर रही थी कि इस पक्ष में कोई हाथ नहीं उठेगा।
यांत्रिक तरीके से वो कमेटी सदस्यों के पास गयी। मंगतू, एडामल, जुगरू और बाकी लोग उनके साथ गये। कुछ समय तक वे सोचते रहे फिर जैनी के निर्देश पर मिलीशिया सदस्यों ने बॉस के दो डंडे लिये और बोकलू और मंगल को पीटना शुरू किया।
जैनी ने मिलीशिया को कार्यभार सौंप दिया था क्योंकि मंगतू ने सावधान किया था कि अगर उन्हें पीटने की लोगों को छूट दे दी गयी तो हो सकता है कि नतीजा उनकी मौत हो जाये। मंगलू ने यह भी निर्देश दिया था कि मिलीशिया सदस्य उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पीटें। मूलतः वह उन्हें पीटे जाने के विचार को पसन्द नहीं करता था क्योंकि उसका मानना था कि इससे उन दोनों में गुस्से की भावना पैदा होगी। फिर भी जन अदालत के फैसले को मानते हुए वह इसे एक तरह की जीत मान रहा था कि बहुमत ने मौत की सजा नहीं देने का फैसला लिया, जैसा कि पार्टी का नजरिया था। जैसे ही मिलीशिया ने उन्हें पीटना शुरू किया भीड़ में से कुछ लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वे आगे छड़ी लेकर आगे आय और खुद बोकलू और मंगल को मारने लगे।
कुछ दूसरे लोग भी छड़ी लेकर उन्हें मारने लगे और कुछ ने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया और कुछ ने ठोकर मारी। दो आदमियों को लोगों ने घेर लिया। उनके परिवार के लोगों में से कुछ लोगों के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे, बस करो, वे मर जायेंगे। कुछ उदासीन भाव से बैठ गये जो मान रहे थे कि यह सजा तो होनी ही थी।
जैनी मंगतू की चेतावनी भूलकर, खड़े-खड़े सब देखती रही। मंगतू के निर्देश पर ढडमिल आगे बढ़ा और पिटाई रोक दी।
’ ’ ’ ’
भारी मन से कन्नी ने खाना बनाने का काम पूरा किया। अंधेरा होने पर हर किसी ने चूल्हे की आग की रोशनी में अपना खाना खाया। उदासी महसूस करते हुए कंधे पर रखे अंगोछे से बोकलू अपने धोये हाथ पोछ रहा था कि उसने मंगल को अपनी तरफ आते देखा जब वह घर के अंागन में आ गया।
खटिया पर बैठकर उसने पूछा, ‘‘तुम सूरज डूबने के बाद क्यों आये ?’’ उसके पास बैठकर मंगल ने आवाज दिया, मैं किसी खास वजह से नहीं आया… यदि मैं उजाले में आता तो मुझे गाँव के एक किनारे से दूसरे तक चलना पड़ता। रास्ते में लोग मिलते । कोई दुआ-सलाम नहीं करता वे अपने चेहरे घुमा लेते या फिर मुझे गिरी नजर से देखते कुछ कोसना भी शुरू कर देते इसीलिए मैं दिन में गलियों में घूमने से डरता हूँ। मैं घर से खेतों की तरफ चला जाता हूँ। बस इतना ही……।
हम क्या कर सकते हैं, सारा गाँव जैसे हमारा बहिष्कार कर दिया हो, ऐसा लगता है। इस तरह हमारी जिन्दगी बदल गयी… बोकलू के शब्द में भारी दर्द था।
‘‘बेकार में परेशान न हों मेरे बेटों। कुछ महीने और बर्दाश्त कर लो। सब कुछ ठीक हो जायेगा.. तसल्ली देते हुए पास की खटिया पर पुराने कपड़े बिछाते हुए एडमिली बोली। कुछ और दिन। गाँव में मुकदमा चले एक महीना बीत चुका है… अब तक कुछ नहीं बदला बोकलू ने जवाब दिया।
बड़ो में हो रही बातों से बेखबर तीन बच्चे आये और खटिया पर लेट गये, और जल्दी सो गये।
उस कमीने उंगल की मीठी बातों से हम जुडुम में शामिल हो गये नहीं तो हम भी गाँव में औरों के साथ रूके रहते चाहे अच्छा बुरा जैसा भी होता।’’ मंगल ने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था।
‘‘अब दोहराने से क्या फायदा ? जब तुम्हारा उससे मिलने का पता चला था तो मैंने तुमसे कहा था कि उस पर यकीन मत करो। मैंने कहा था कि चाहे जिये या मरे हमें गाँव वालों के साथ रहना चाहिए । क्या तुमने सुना ? तुमने सोचा कि तुम बेहतर जिन्दगी जियोगे और देखों अब क्या हुआ।’’ कन्नी ने निराशा में क्या जब वह बच्चों को कम्बल में ढँग रही थी।
कुछ पल दोनों उसकी बातों को स्वीकार करते हुए खामोश रहे।
‘‘बेवकूफी में हमने उसकी बातें मान ली। हमने हमेशा के लिए जुडुम में रहने की योजना नहीं बनायी थी। ऐसा होता तो हम तुम्हें भी साथ आने को कहते। लेकिन एक बार जब हमने समर्पण कर दिया और शिविर में हमारा नाम दर्ज हो गया तो उंगल ने हमें भरोसा दिलाया कि यदि हम घर वापस लौटते तब भी जुडुम हमें कुछ नुकसान नहीं पहुँचायेगा। लेकिन वहाँ शिविर में जब हमारा नाम दर्ज हो गया तो उसने हमें वहाँ यह कहकर रखा कि यदि हम वापस लौटे तो नक्सली हमें मार डालेंगे…….. उसके बाद कठपुतलियों की तरह हम उसके इशारे पर नाचे’’ ….. से मंगल ने सफाई दी।
कन्नी के लिए कुछ भी नयी बात नहीं थी। कई बार उसका पति उसे बता चुका था। कुछ पल के लिए वह चुपचाप खड़ी रही और फिर घर के अन्दर गयी और एक बच्चे को लेकर आयी जो उसके कंधे पर सो रहा था। जल्दी ही हर कोई सो गया। केवल बोकलू और मंगल बातें करते रहे।
‘‘कभी – कभी मैं महसूस करता हूँ कि वही अच्छी या बुरी हर हालत में टिके रहना बेहतर होता। मैं यहाँ बहिष्कार की जिन्दगी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।’’ बोकलू बोला।
‘‘अरे छोड़ों, हमने एक बार गलती की। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम हमेशा के लिए गलत रास्ते पर चलें। मंगल का जवाब था। लेकिन हर कोई हमें किस नजर से देख रहा है ? बुरी से बुरी…..।’’
आधी रात बीत चुकी थी फिर भी दोनों अपना दर्द और गम साझा करते हुए बात करते रहे।
’ ’ ’ ’
यदि उसी वक्त हमने उन्हें मार डाला होता तो अच्छा होता। क्या तुमने हमारी बात सुनी, हमने इतना ज्यादा निवेदन किया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा।’’ गुलाबी, एडामल से यह कह रही थी उसके चेहरे पर असहायता, हताशा और गुस्से के भाव थे।
खटिया पर बैठे एडामल ने कुछ जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि सिर भी नहीं हिलाया।
‘‘वे कह रहे थे कि वे बदल गये हैं और इन लोगों ने भोलेपन में उनका यकीन कर लिया। कुमली ने कहा वे कुछ योजना बनाकर ही आये थे लेकिन हमने पूरी तरह उन पर यकीन नहीं किया, सही है ? हमने उन पर नजर रखी। जब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है तो वे पलायित हो गये। सोमल ने बात आगे रखी।
कौन जाने वे अब कौन सा अत्याचार करेंगे…।
‘‘हमने उनका जमकर विरोध किया। हमने जोरदार तरीके से उन्हें मौत की सजा देने की दलील दी।…। हमारे खिलाफ उनके मन में दुर्भावना हो सकती है। कुमली आगे कहती गयी।
गुलारी ने कहा ‘‘हमने उन्हें उस समय जाने दिया जब वे हमारे हाथों में थे। पता नहीं ऐसा मौका फिर से हमें मिलेगा ?
जो हुआ उसे वापस लाया नहीं जा सकता। ऐसा सोचते हुए जैनी ने कहा, मैनें भी यह महसूस किया था कि अच्छा होता यदि हम उन्हें उसी वक्त मार डालते लेकिन हम क्या कर सकते है ? हमने सबकी सुनी और उन्हें जाने दिया…..।
लगभग सौ लोग उनके घर के बाहर जमा हो गये थे, हर कोई अपनी राय रख रहा था। पड़ोसी गाँव से लौटने के दौरान जुगरू को जब हालात का पता चला तो इस हंगाने के बीच आया। बोकलू के घर पर सबकी बात सुनने के बाद वहाँ सीधे पहुँचा। वहाँ पहुँच कर एडामल ने खटिया पर पसर कर तौलिया से पसीना पेछा और पूछा ‘‘वो कब यहाँ से भाग गये।’’ ज्यादा बात विस्तार से उसे सब पता था फिर भी सबसे इसकी पुष्टि कराना चाह रहा था।
कन्नी और एडमी की तरफ एडामल ने इशारा किया जो घर के सामने एक पेड ़के नीचे सिमट कर बैठी थी और डर से कॉप रही थी।
‘‘उनसे पूछा’’
जुगरू ने उनके चेहरे की ओर देखकर पूछा क्या तुम्हें कुछ सन्देह हुआ था कन्नी ?’’
धीरे से उसने सिर उठाया और एक पल के लिए जुगरू की ओर देख सिर झुका लिया। वह बोलने की हालत में नहीं थी; उसका दिल विश्वासघात के बोझ से भरा था। वह किसी को अपना मुँह नहीं दिखाना चाहती थी। फिर भी उसे बोलना ही था।
‘‘कल रात के खाने के बाद मंगल आया था। इस खटिया पर बैठकर वे दोनों बातें कर रहे थे। मेरी सास खटिया पर सो गयी। इस खटिया पर पर बच्चे सो गये। मैं छोटे के साथ अन्दर सो गयी। आधी रात के बाद मैं नित्य कर्म के लिए उठी तो देखा खटिया पर कोई नहीं है। बाकी मैं कुछ भी शक नहीं कर रही।
कहते-कहते वह रोने लगी और आँसू बहने लगे। विश्वास टूट जाने का दर्द उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसने खुद को संभालते हुए आगे कहना शुरू किया, ‘‘मैंने सोचा कि वह भी नित्य कर्म के लिए बाहर गया होगा… मैं वापस सो गयी। सबेरे जब मैं उठी तब भी वो वहाँ नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानती। हमें अचरज हुआ कि वह कहाँ चला गया। हमें लगा कि वे लौट आयेगा इसलिए हमने इंतजार किया। जब वो हमारे ……. जीने के समय तक नहीं लौटा तो मैंने अपनी सास से एडमिल के पास जाकर उसे बनाने को बोला।
अपनी भावनाओं के भारी दबाव के आगे वो बोल नहीं सकी।
‘‘रात में कुछ समय के लिए मैं उठी थी और उन्हें बातें करते हुए सुन रही थी लेकिन फिर कोई आवाज नहीं सुनी तो मैंने सोचा कि वे सो गये हैं… वह ऐसा करेगा यह तो मैंने सोचा ही नहीं था।’’ एडमी के शब्दों में उसका दर्द उभर कर सामने आ गया।
अपनी माँ के पीछे बैठे और सात साल के लड़के थोड़ा बहुत ही समझ सके थे क्यों इतने सारे लोग उनके घर के सामने जमा हैं, क्यों उनकी माँ दादी व्यथित हैं। शोर गुल के वातावरण में डेढ़ साल का छोटा बच्चा परेशान होकर रोये जा रहा था। जब भी बच्चा चिल्लाता उसकी दादी उसे अपनी गोद में भर उसे चुप कराने में लग जाती। कुछ महीने पहले हर कोई इस छोटे पर ध्यान देता था लेकिन अब कोई उसे छू भी नहीं रहा था।
‘‘क्या तुमने कुछ ध्यान दिया ? क्या पिछले कुछ दिनों में उसमें कुछ बदलाव आया था ? जुगरू ने पूछा कन्नी ने जवाब दिया,’’ नहीं हमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। वह ठीक ठाक लग रहा था।’’
जुगरू ने फिर पूछा, ‘‘जब मंगल आया तब दोनों क्या बातें कर रहे थे ? क्या तुमने कुछ सुना ?’’
‘‘मैंने उनको यह कहते सुना था कि गाँव में कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। कल तक भी लग नहीं रहा था। कि वह कुछ ऐसा करने की सोच रहा है। कन्नी ने कहने के साथ फिर से सिर झुका लिया।
एडमी महसूस कर रही थी कि उसके बेटे को मंगल ने ठुकराया है। अपने बेटे पर वह दिल से भरोसा करती थी।
सोमवती ने आगे कहा, ‘‘उन्हंे एहसास हुआ होगा कि उन पर कोई भरोसा नहीं करता है और सोचा होगा कि दिन कहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है।
सोनल ने प्रोत्साहित किया, ‘‘यदि तुम कुछ जानती हो तो चिल्लाओ मत! हमें सच-सच बता दो।’’ कुछ और आवो भी गूँजी, हाँ बताओ! ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ न मालूम हो।’’
कन्नी रोने लगी, ‘‘इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते।
कृपया हमारा यकीन करें। अब तक जिस दुःख, दर्द को वह संभाल रही थी वह अब फूट पड़ा। साथ ही एडमी भी जोर-जोर से रोने लगी। अपनी माँ और दादी को राते देखकर बच्चे अपनी माँ से चिपक गये और वे भी रोने लगे।
‘‘शान्त हो जा बहन ? हमें तुम पर विश्वास है। अब शांत हो जा।’’ गुलारी ने कहा। अपने बच्चे को जल्दी से गोद में उतार कर वह कन्नी के पास बैठ गयी और उसे तसल्ली देने लगी। कन्नी की बुरी हालत पर गुलारी सहानुभूति महसूस करने लगी। उसने सोचा उससे शादी करके सबके सामने शर्मनाक स्थिति में बैठना, कितनी खराब तकदीर है।’’ कन्नी और गुलारी अच्छी दोस्त रही थी लेकिन जबसे वोकलू जुडुम में शामिल हुआ था, तबसे गुलारी ने कन्नी से दूरी बनाये रखी। पंचायत के बाद दोनों एक दूसरे से बोली नहीं थी। गुलारी द्वारा कन्नी को तसल्ली देते हुए कुछ और लोग भी तसल्ली देने लगे। कुछ लोग बच्चे को संभालने लगे।
फिर कुछ लोग अब भी उन्हें नफरती निगाहों से देखते हुए सोच रहे थे कि ‘‘क्या सच में ये कुछ नहीं जानती ? ऐसा कैसे हो सकता है।’’ गुुलारी ने अपने दर्द की तुलना कन्नी के दर्द से की। गुलारी हमले का शिकार बनी थी लेकिन उसके पति ने उसे अपनाते हुए वापस घर में रखा था और गाँव वाले भी उसके साथ खड़े थे। उसका सिर शर्म से कभी नहीं झुका। लेकिन कन्नी की स्थिति अलग थी। उसका पति जिससे हर सुख-दुःख का साथी होने की उम्मीद थी, वह चला गया था और अपनी कार्यवाहियों के लिए पत्नी को चोट पहुँचने तथा झेलने के लिए छोड़ गया था। पति के अपराधों के लिए अब वो सिर झुकाये थी। सबसे बड़ी मुसीबत थी कि अब भी कुछ लोग उस पर अविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे। कभी दुलारी खुद को कटु अनुभवों की वजह से सबसे ज्यादा अभागिन मानती थी लेकिन कन्नी की तुलना में खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगी। दुलारी सोचती थी कि मंगल की पत्नी भी कन्नी की तरह रोती होगी।
’ ’ ’ ’
सही में चाचा! क्या आप सोचते हैं हम आपसे झूठ बोलेंगे ? बोकलू ने कैरी-उंगल से कहा जो उनके सामने बैंच पर बैठा था। ‘‘हम बस यहाँ रहते-रहते ऊब गये थे और सोचा कि एक बार गाँव हो आयें। हमने अपने बच्चों को नहीं देखा था। हमारा इरादा वहाँ रह जाने का नहीं था चाचा! यदि हम वहाँ रह जाना चाहते तो वापस क्यों आते।’’ वह आगे बोला मंगल बोला ‘‘क्या आप हमारे बारे में सब कुछ जानते है चाचा ? हम क्या आपसे झूठ बोलेंगे ?’’
पिछले आधा घण्टे से वे तीनों बातें कर रहे थे। आखिरकार उंगल को बोकलू और मंगल की बातों पर यकीन हो गया।
‘‘तुम लोगों को मुझे पहले बताना था।’’ उंगल ने कहा।
‘‘अगर हम आपको पहले बताते तो आप हमें जाने नहीं देते।’ इसलिए आपको बिना बताये हम चले गये। बोकलू ने जवाब दिया।
‘‘ठीक है मैं यकीन करता हूँ लेकिन हो सकता है पुलिस अफसर न करे। तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताना होगा – वहाँ तुमने क्या किया, किससे मिले, सब कुछ’’बताने को कहा।
बोकलू और मंगल दोनों ने सहमति में सिर हिलाये। ‘‘और तुम दोनों इस तरीके से दुबारा नहीं भागोगे, क्या ऐसा करोगे ?
‘‘चाचा! अब हम यहाँ से भागेंगे तो गाँव में कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। यह बहुत बड़ी बात है कि गाँव में हमें मौत के घाट उतारने के बजाय जिन्दा छोड़ दिया गया ? हमें डर – डर कर जीने तथा हर किसी से जान की भीख माँगने के बजाय यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हैं।’’ तो फिर इस बार बच्चों को क्यों नहीं साथ लाये ? उंगल ने पूछा।
चाचा औरते नहीं सुनती। वे डरती है कि नक्सली उन्हें मार डालेंगे?’’ मंगल ने बताया।
‘‘हमने उनसे कहा कि वे नहीं आयीं तो हम दूसरी शादी कर लेंगे फिर भी अभी तक उन्होंने हमारी बात नहीं मानी चाचा। हमें अब अपना रास्ता खुद तय करना है। बोकलू आगे बात।
‘‘मैंने तुम लोगों से दूसरी शादी यहाँ करने को कहा था लेकिन तुम्हारे साथियों ने जोर दिया था कि तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारा साथ देंगी। ‘‘उंगल ने जवाब दिया।
बोकलू बोला, ‘‘हमने सोचा कि ऐसा होगा।’’
‘‘ठीक है हम लोग पुलिस स्टेशन चले और पुलिस अफसर से बात करें। फिर भी वे तुम्हें फौरन एस0पी0ओ0 शायद नहीं बनाये। लेकि हताश मत हो। यहाँ सबके साथ शिविर में रहो।
उंगल बोला और अपनी बन्दूक लेकर उठ खड़ा हुआ।
चाचा यहाँ आइये। माँस… जरा चखिये, मंगल बोला उसने भुने हुए माँस का पत्तियों से लिपटा एक बंडल हाथ में थामा हुआ था जिसे वह मंगल के सामने पेश कर रहा था। मंगल घर के सामने एक बेंच पर बैठा हुआ था। मंगल के पीछे बोकलु भी तीर-धनुष लिए खड़ा था जबकि मंगल के पास एक कुल्हाड़ी और गोफन था।
पशु-पक्षियों का शिकार वे तीर-धनुष से करते थे। फिर भी विभिन्न पक्षियों के शिकार के लिए विभिन्न तीर इस्तेमाल किये जाते। पक्षियों को मारने के लिए गोफन का इस्तेमाल भी करते थे। जब गिलहरियाँ पेड़ों की खोह में छिप जाती तो वे पेड़ों को काटकर उन्हें पकड़ लेते। इसलिए उनके पास शिकार पर जाते हुए हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी।
उत्सुकता से उंगल ने पूछा; किस तरह का माँस यह है ?
‘‘पक्षियों का’’ मंगल ने जवाब दिया।
बिना जवाब का इंतजार किये उंगल ने जल्दी से बंडल खोला माँस का एक टुकड़ा उठाया और अपने मुँह में रखा। जल्दी ही वह चबा गया और बोला, ‘‘यह बढ़िया है।’’ साथ ही इससे टुकड़ा उठा लिया।
आमतौर पर आदिवासी माँस पसन्द करते है लेकिन उंगल की आसक्ति चरम पर थी। अपनी तीव्र इच्छा शान्त करने के लिए, वह जब गाँव में था, तो ज्यादातर समय शिकार करने में बिताता था। शिकार में आ जाने के बाद हालांकि वह मानवों का शिकार करने में व्यस्त हो गया और पशु-पक्षियों का शिकार करने का समय नहीं मिला। फिर भी उसकी इच्छा थी लेकिन जंगल में अन्दर तक अकेले जाने में खतरा था। शिविर की सड़क काफी करीब थी और कई लोग सड़क के करीब रहते शिकार में अपनी किस्मत आजमाते। उन्हें कभी-कभी ही कुछ मिल पाता। उंगल के आ जाने के बाद उन्हें गाँव में धावा मारने पर नियमित रूप से बकरी, सूअर, मुर्गा बत्तख इत्यादि मिलने लगे। आमतौर पर बिना माँस के उसका कोई दिन नहीं बीता था। लेकिन पत्तियों में लपेटकर आग में भुनकर मछली और पक्षी माँस की तो बात ही कुछ और थी। लम्बे समय बाद इसका स्वाद उंगल ने चखा था। दो माँस में टुकड़ों को खाने के बाद वह उन्हें लेकर अन्दर चला गया। उन्हें शराब के साथ चखने के लिए बैचेन था।
बोकलु और मंगल चले गये।
उस दिन के बाद से उंगल के लिए माँस, पत्तियों में लपेट कर भुना मछली या पक्षी माँस ले आना बोकलु और मंगल का रोज का काम हो गया। घर में बने माँस से ज्यादा मजा उंगल को इसमें आया।
एक दिन बोकलु से पत्तियों का बंडल लेते हुए उंगल ने कहा, ‘‘तुम लोग शिकार करने का बड़ा काम कर रहे हो।’’
हमारे लिए बचा ही क्या है ? बिना कुछ करे हम एक किनारे कैसे बैठे रह सकते हैं ? इसलिए हम लोग चक्कर लगाते जा रहे है। बोकलु ने जवाब दिया शिकायती लहजे में मंगल बोला, ‘‘अभी तक आपने हमें एस0पी0ओ0 नहीं बनाया।
‘‘चिन्ता मत करो। अगले महीने में तुम्हें फिर से एस0पी0ओ0 बनवा दूँगा यहाँ मेरे कहे को कोई नकारने की हिम्मत किसी में नहीं है। उंगल ने आश्वस्त किया।
बोकलु और मंगल के चेहरे चमक उठे। ‘‘हम जानते है चाचा। आपके मुँह से निकली बात को नकारने की हिम्मत कोई पुलिस अफसर नहीं करेगा। हमारी शिकायत यह है कि हमारे लिए आपने मुआवजा नहीं तय किया, वे बोले। गर्वीली मुस्मकान के साथ उंगल ने बचा हुआ माँस लिया और अन्दर चला गया।
अगली शाम को बोकलु और मंगल नहर की तरफ गये। शिविर में आये उन्हें लगभग दो महीने हो चुके थे। रास्ते में उनकी उंगल से भेंट हो गयी। उसने पूछा ‘‘किधर जा रहे हो ?’’
बोकलु और मंगल उससे बोले,’’ कुछ केकड़े पकड़ने हम लोग जा रहे हैं।’’
उन्हें रात में आसान है। उंगल ने कहा। ‘‘अब भी ठीक ठाक समय है।’’ बोकलु ने जवाब दिया। एक पल सोचने के बाद उंगल बोला, ‘‘ठीक आज मैं भी साथ चलूँंगा।’’
‘‘क्यों चाचा क्या आप भी केकड़े पकड़ने के मूड में है। बोकलु ने हँसते हुए पूछा।
बिल्कुल ! काफी दिन बीत गये जब मैं उन्हें खोजने गया था।’ उंगल ने जवाब दिया।
ठीक है हमें चलना चाहिए। आज हमें काफी मात्रा में मिलेंगे। अपनी पत्नी से पकाने का बढ़िया इन्तजाम करने को बोल दे।’’ मंगल बोला तीनों हँसते हुए नहर की तरफ चले जब वे नहर की तरफ पहुँचे, मंगल और बोकलु ने अपने धनुष, तीर तैयार कर लिए एक बड़े पेड़ के लिए कुल्हाड़ी ली और केकड़े पकड़ने के लिए चट्टान उठाने लगे। उंगल उनके साथ मजा लेने के लिए ही आया था उन्हें केकड़े पकड़ने देख रहा था। उसने इस शिकार करने में हिस्सा नहीं लिया।
उसी समय मंगल ने एक बड़ी चट्टान उठा ली, अपने घुटनों के बल झुका और केकड़े खोजने नीचे चला गया। कुछ समय बाद उसने आवाज दी, ‘‘अरे बोकलु, इस चट्टान को थोड़ा ऊपर उठाओ…. नीचे एक बड़ा केकड़ा है।’’ बड़ा केकड़ा खोज लेने का उत्साह उसके चेहरे पर था। बोकलु ने दोनों हाथों से चट्टान उठाने की कोशिश की लेकिन ठीक से पकड़ नहीं बना पाया।
थोड़ा सा और ! मेरे हाथों को नीचे संभालने की जरूरत है ‘‘मंगल ने निर्देश दिया।’’
चट्टान बहुत बड़ी है और मैं पकड़ में नहीं ले पा रहा हूँ। चाचा यहाँ आइये और हमारी मदद कीजिए।
उंगल ने अपनी बन्दूक एक चट्टान पर टिकायी और नीचे झुक कर दोनों हाथ चट्टान के नीचे ले आया।
बोकलु बोला, चाचा नीचे आप थामें रहो ऊपर मैं सम्भालता हूँ उंगल ने थोड़ा अपना सिर झुकाया और चट्टान के नीचे अपने हाथ रख दिये।
धीरे से बोकलू ने अपनी पकड़ चट्टान से हटा ली।
’ ’ ’ ’
सबेरे-सबेरे गाँव के दाहिनी तरफ के आम के पेड़ों के पास बच्चे-बूढ़ों को छोड़कर लगभग सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गये थे। अभी सूरज निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। हालांकि नवम्बर का महीना था फिर भी काफी ठण्डक थी। लेकिन किसी को ठंड की परवाह नहीं थी। वे ताली बजा रहे थे और हँस रहे थे। सभी वहीं सामूहिक फसलों की जुताई के लिए एकत्र हुए थे।
जुड्रम की तबाही के बीच उन्होंने अपनी जिन्दगी खतरे में डाल कर अपने खेतों की हिफाजत की थी और अब वे सन्तुष्ट होकर उसकी देखभाल कर रहे थे। विकास कमेटी से अन्य तथा भीम्मल वहाँ एकत्र लोगों को ग्रुप में बाँट रहे थे। जल्दी ही हर कोई नजदीकी फसल के खेतों में जा रहा था।
इसी समय किसी ने कहा, ‘‘मिलीशिया आ रहा है…! दूसरा बोला, ‘‘ऐसा लग रहा है कि वे किसी को लेकर आ रहे हैं…!
अरे ये बोकलू और मंगल है ….!
पल भर के लिए कोई कुछ नहीं बोल सका। थोड़ा हंगामा शुरू हो गया।
‘‘उन्होंने चोर पकड़ लिए।’’ सोमल चिल्लाई’’
‘‘अब वे बच कर जा नहीं सकते।’’ मीम्मत बोला।
एडामल ग्रुप से बाहर निकला। एडामल के सामने मिलीशिया ने बोकलु और मंगल को पेश किया।
एडामल ने पूछा ‘‘कहाँ से पकड़ा ?’’
हमने उनको गाँव की तरफ आते हुए पकड़ा…। एक पल के लिए एडामल को समझा में नहीं आया कि क्या कहे। दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। गुस्सा उसके भीतर था। उसे याद आया कि कैसे उस दिन पंचायत में हर कोई उन्हें मार डालना चाहता था लेकिन हर किसी के राजी कर लिया कि उन्हें जाने देना चाहिए जिसकी वजह से आगे लोगों के सामने उन सबके सिर झुक गये थे।
एडामल के कुछ कहने से पहले वहाँ हर कोई फौरन अपनी बात करने लगा।
ग्रुप में कन्नी भी थी। अपने पति को देख उसके पैर काँपने लगे। उसका दिल धक-धक करने लगा। खड़े न रह पाने की वजह से वह एक तरफ किनारे बढ़ी और गिर पड़ी।
मंगल की पत्नी को भी वहाँ होना था लेकिन एक दिन पहले वह पड़ोसी गाँव में चली गयी थी।
हर पल भीड़ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। किसी के कहने का कोई मतलब नहीं था, इससे वे सन्तुष्ट नहीं थे। वे अपने हाथों से कार्यवाही करना चाहते थे।
उनके शरीर को दो चोट पहले ही लग चुकी थी। एडामल ने कहा, ‘‘रूको रूको…. मुझे जरा बात कर लेने दो।’’ बात करने के लिए क्या है ? उन्हें मार डालो और बस काम खत्म! कुमली बोली हाँ। उन्हें अभी मार डालो, बात करने से क्या फायदा ? एक साथ कई लोग चिल्लाये। जुगरू जोर से बोला ‘‘अरे! क्या आप एक पल के लिए शान्त रहेंगे ?
‘‘शांत रहना ? आप उनसे बात करेंगे, वे कुछ कहानी सुनायेंगे और आप उन पर यकीन कर लेंगे।
गुलारी बोली। उसकी आवाज गुस्से, हिकारत और ताना मारने के भाव से काँव रही थी। ‘‘बिल्कुल यदि आप उनसे बात करेंगे तो वे कहानियाँ सुनाने के अलावा क्या करेंगे।’’ एथी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
कन्नी के दिमाग में उथल-पुथल हो रही थी। क्या उन्हें मार डालेंगे, क्या उसकी आँखें जान की भीख वह लोगों से माँग सकती है, उसके पूरे शरीर में उथल-पुथल मच रही थी।
कुछ लोग कन्नी की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। गुलारी ने कन्नी की तरफ देखा अरे तुरन्त अपना चेहरा घुमा लिया। वह उसे ऐसी दुःखी हालत में नहीं देख पा रही थी। पिछले दो महीनें में गुलारी और कन्नी के बीच पहले से ज्यादा गहरी दोस्ती हो गयी थी। गुलारी ने हर मुमकिन तरीके से कन्नी का साथ दिया था। पहली पंचायत के बाद कन्नी कभी-कभी गुलारी से इस वजह से गुस्सा हो जाती थी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि गुलारी उसके पति से उस दौरान नफरत कर रही थी जब वह एक महीने घर पर था। लेकिन हाल में कन्नी ने गुलारी के दोस्ताना दिल की ज्यादा गहराई को समझ लिया था।
लोग क्या कह रहे है सबको सुनाई दे रहा है ठीक है ? बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाये… एडामल ने कहा।
‘‘दया करके पहले हमारी बात सुन ले फिर जो चाहें सो कर लें बोकलु ने बात रखी।
कुमली गुलारी से बोली ‘‘देख, अब वे कहानियाँ सुनाना शुरू कर देंगे।
गुलारी ने सहमति के सिर हिलाया लेकिन उसकी नजरे दोनों आदमियों पर टिकी रही।
हिचकिचाते हुए बोकलु ने बोलना शुरू किया ‘‘हम यहाँ से चले गये लेकिन एस0पी0ओ0 के रूप में काम नहीं किया।
यदि उन्होंने एस0पी0ओ0 के रूप में काम नहीं किया लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ऐसा करना नहीं चाहते थे। ‘‘सोमाल ने जोर से कहा।’’
‘‘यदि वे एस0पी0ओ0 नहीं बने तो क्या हुआ ? क्या वे सोचते है कि उनके उंगल के चारो तरफ नजदीकी से घूमते रहने का पता हमको नहीं है ?
सबको शांत रहने का इशारा करते हुए एडामल ने कहा, ‘‘आगे बोलो।’’
‘‘हम बेकार में डर गये थे और कैरी उंगल की बातों में आ गये थे। हमने भयानक गलती की। लेकिन उस गलती का एहसास दोने पर हम वहाँ से भाग आये। हालांकि हमारी रक्षा की गयी लेकिन किसी ने हम पर भरोसा नहीं किया। हमारा सामाजिक बहिष्कार हुआ था…. इसलिए हमने इस बारे में सोचा कि आप लोगों का भरोसा पाने के लिए हम क्या करें….।
बोकलु रूक गया। ‘‘हर किसी का भरोसा तुम पर हो जाये, तुम्हें फिर से भाग जाना चाहिए’’ कुमली ने कटाक्ष से कुछ लोग हँसने लगे।
न केवल भाग गये बल्कि कैरी उंगल के इर्द-गिर्द चक्कर लगाते रहे, उसके लिए माँस पकाते रहे… एथी ने आगे कहा।
अपनी बात कहने के बाद बोकलु ने मंगल की तरफ देखा। उसका इशारा समझ कर उसने बॉयें हाथ से अपने कंधे से बैग उतारा और दाहिने हाथ को अन्दर डालकर उसमें से कुछ बाहर निकाला।
यह है ! हर कोई, जो कुछ कहने या भला बुरा कहने जा रहा था, हक्का-बक्का रह गया। उनकी आँखें फैल गयी। हर किसी की सांस थम गयी।
मंगल ने एक सिर पकड़ा था। एक मानव सिर’’ पास की एक चट्टान पर उसने उसे रख दिया।
कैरी उंगल का सिर… किसी ने कहा।
‘‘हाँ हाँ’’ कई लोग चिल्लाये जो अपनी खुशी छिपा नहीं पाये। यह वो आदमी है जिसने हमें आप सबसे दूर कर दिया था….. यह वह है जिसने हमारे गाँव में बर्बादी लायी थी….. इसलिए हमने उसे मार डाला। हम पर अब तो भरोसा करो….।
एडामल ने पूछा, तुमने उसे कैसे मारा। उसी समय उसने अपने दोनों हाथ कंधों के पीछे कर लिए थे जो हुआ वह अपनी प्रसन्नता उस पर छिपा नहीं पा रहा था। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने उस आदमी को मारने की कई कोशिशें की लेकिन विफल रहे थे।
‘‘हमारे साथ वह शिकार पर आया। दो महीनों से हमें इस मौके का इंतजार कर रहे थे। हमने उससे एक पत्थर थामने को कहा और जैसे ही उसने ऐसा किया हमने एक कुल्हाड़ी उठायी और एक ही वार में उसका सिर अलग कर दिया।’’
खबर सुनकर बूढ़े, पुरूष, औरतें और बच्चे गांव से दौड़े-दौड़े आये और शोर मचाने लगे।
एकाएक सब लोग जोर से बोलने लगे। जैनी बोली ‘‘सब लोग बैठ जायें और एक-एक कर के बोलें।’’ चार-पाँच बार ऐसा गम्भीरता से कहने पर भीड़ धीरे-धीरे शांत हो गयी। कैरी उंगल द्वारा अपने ऊपर किये गये अत्याचारों कोपार करके उनके दिल गुस्से से सुलग उठे।
इसके साथ ही उन्हें इस बात का संतोष भी हुआ था कि आखिरकार उसका सफाया हो गया।
एक बूढ़ी औरत आगे आयी और कहा, उसने मेरी दो बकरियाँ चुरायी थी।
एक जवान औरत ने जोड़ा… ‘‘मेरी चार मुर्गियां उठा ले गया और इस तरह एक के बाद दूसरा अपनी शिकायतें बताने लगा।
‘‘उसने हमारे घर जलाये….
‘‘जब फसल तैयार हो गयी थी उसी समय हमारे चार एकड़ में फसलों को आग लगा दी…..
‘‘उसने मेरे बेटे को इतना मारा कि खून निकलने लगा।’’
‘‘वो मेरे बेटे का अपहरण कर शिविर में ले गया और उसे मार डाला।’’
‘‘उसने मेरे पति को मार डाला’’
‘‘उसने मेरे बेटे की जिन्दगी तबाह कर दी…..
‘‘उसने मेरी बेटी के कपड़े उतारे और नंगी परेड करवायी….। उनका गहरा दर्द उनके शब्दों में उनके आँसुओं के गुस्से में बाहर आ गये। हर कोई फिर से बात करने लगा। अब रूक जाइये एडामल ने दो-तीन बार जोर से कहा और भीड़ शांत हो गयी।
सिर का क्या किया जाये इस बारे में कुछ बातचीत के बाद जैनी ने सुझाव दिया।
‘‘इसे सड़क पर फेंक दिया जाये।
’ ’ ’ ’ ’
एक हफ्ते बाद एडमिल, जैनी और जुगरू कमांडर मंगने से मिले जो पड़ोसी गाँव में था। उसे बताया कि बोकलु और मंगल ने कैरी उंगला को मार डाला था।
मंगलू ने ध्यान दिया कि उनकी आवाजों में क्रोध-आक्रोध और उत्तेजना है। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मंगतू खुश होगा और उनके अच्छे काम के लिए उनकी तारीफ करेगा। फिर भी मंगतू कुछ उदास लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और हर चेहरे पर नजर दौड़ाई।
‘‘सिर के साथ आपने क्या किया।’’
उदासी भरी आवाज में उसने पूछा।
‘‘हमारे लोगों ने उसे उठाया और सड़क पर फेंक दिया। पुलिस उसे उठाकर ले गयी।’’ जैनी ने कहा।
‘‘यह एक बड़ी समस्या हो गयी है। दुश्मन हर मुमकिन तरीके से पार्टी, जनताना सरकार, हमारे जनसंगठनों की छवि एक राक्षस की तरह पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है।
क्या उसने बहुत सारे जुल्म नहीं ढहाये, उसने हमारे गाँव को नरक बना दिया, क्या ऐसा नहीं किया ? इसके अलावा हमारी मिलीशिया ने उसे मार डालने का फैसला लिया था। ‘‘जैनी ने जवाब दिया।’’
उसी समय रसोईघर से उन चारो के लिए चाय आ गयी।
‘‘कामरेड। हमारी जनताना सरकार एक हिंसा रहित दुनिया बनाने के लिए गठित हुई है। यह उच्च मूल्यों के लिए काम करती है। ‘‘एक आँख के बदले एक आँख का पुराना तरीका अब चलन में नहीं रहा। हम वो लोग है जो इतिहास तथा द्वन्द्वात्मक तरीको को समझते हैं। हम कम्युनिस्ट हैं। बोकलु और मंगल को सजा देने के बाद क्या हमने उनकी देखभाल की ? गाँव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया; हमारी जनताना सरकार को क्या करना चाहिए ? सजा के बाद हमें उन्हें अपने कामों के जरिये सुधरने का मौका देना चाहिए। हमने उन्हें क्या काम दिया? जनता के बीच से दुश्मनी हटाने के लिए हमें उन्हें अपनी सामूहिक खेती और मिलीशिया में शामिल करना चाहिए, उनके व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए और खुद में सुधार लाने में उनकी मदद करनी चाहिए। क्या हमने उनके लिए ऐसा कुछ किया ? मंगतू ने रूक कर चाय खत्म की।
नहीं दादा, हमने इस तरीके से नहीं सोचा एडामल ने स्वीकार किया।
वे अलग-थलग पड़ गये… कैरी उंगल के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्या ऐसा नहीं था ? अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उन्होंने कैरी उंगल की हत्या करने का फैसला लिया… उंगल यदि उन्हें मार डालता तब ? जनताना सरकार को और ज्यादा लोगों को जुटाने, खुद को मजबूत करने की जरूरत है। व्यक्तिगत फैसलों के बदले हमारे पास एक सांगठनिक ढाँचा है। किसी भी कार्यभार के बारे में विचार विमर्श हो, फैसला होने और क्रियान्वयन में सरकार की पहल कदमी हो। हमें अपने काम-काज के तरीके बेहतर बनाने की, व्यक्तिगत आवेश की जगह सामूहिक फैसले पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है। गंगतू ने कहा।
‘‘उस तानाशाह काबोझ हट गया। क्या ऐसा नहीं हुआ ? जैनी ने बीच में रोका।
‘‘हाँ लेकिन बोकलु और मंगल को ऐसा जन मिलीशिया के साथ मिलकर करना चाहिए और यह एक सामूहिक फैसला होना चाहिए। सिर काटना हमारा तरीका नहीं है…. हम अपने आवेश या गुस्से में काम नहीं करते।
हम अपने ऊपर थोपी हिंसा रोकने के लिए कार्यवाही करते है और वो भी उसी वक्त जब जरूरी हो जायें और न्यूनतम खतरे से किया जाये। हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। हम उतने ही पवित्र है जैसे जंगल। हम जनताना सरकार के माध्यम से एक नयी दुनिया बना रहे हैं। सिरों को अलग कर देना हमारा रास्ता नहीं है। इस अन्तर को लोगों तथा अपने सदस्यों को विस्तार से समझाने की जरूरत है। मंगतू ने निष्कर्ष निकाला।
शेष तीनों ने अपनी विदाई की और गाँव में वापस जाने की यात्रा शुरू कर दी।
उन्हें उम्मीद थी कि मंगतू उनकी तारीफ करेगा। शुरू में इस तरह से बात करना, उन्हें सही नहीं लगा। वापस आने के रास्ते में उन्होंने सारा विचार विमर्श किया।
जैनी ने खुद के बारे में सोचा, ‘‘ऐसे मामलों में हमें डिवीजन के कानूनी विभाग के सारे लोगों की मीटिंग बुलाने का आग्रह करना चाहिए।
एडामल को आश्चर्य हुआकि बोकलु और मंगल को क्या कार्यभार सौंपा जाये ?
जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह समाहित नहीं करके जुगरू का दिमाग सोचना बन्द करने जैसा लग रहा था।