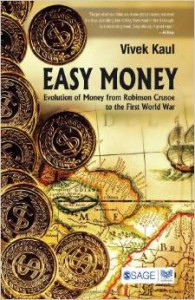बीते माह की 14 तारीख को फिलीपीन्स के ‘वालेन्जुएला’ शहर में हवाई चप्पल बनाने वाली एक फैक्टरी ‘केन्टेक्स’ में आग लग गयी। और इस आग में झुलस कर 72 लोगों की मौत हो गयी। इसमें ज्यादातर महिलाए हैं। 69 लाशें तो इस कदर झुलस गयी हैं कि उन्हें पहचानना अब संभव नही रहा। इसलिए मरने वालों के रिश्तेदारों के डीएनए लिए जा रहे हैं। डीएनए सैम्पल देने के लिए लाइन में लगे मरने वालों के रिश्तेदारों को रोते हुए मीडिया पर देखना बहुत ही ह्दय विदारक है।
अफसोस है कि ‘सूचना क्रान्ति’ और ‘मीडिया-वैश्वीकरण’ के इस दौर में जब हमें ना चाहते हुए भी दुनिया भर के ‘सेलेब्रेटीज’ के खांसने और छींकने की भी खबरें तुरन्त मिल जाती है, वही यह घटना मुख्यधारा की मीडिया से गायब रहा। अभी भी गायब है।
खैर इसके बाद की कहानी वही है जो हमेशा होती है। यहां पर मजदूरों की सुरक्षा का कोई भी उपाय नही था। यहां तक की आग पर काबू पाने का औपचारिक उपकरण भी नही था। राना प्लाजा की तरह ही यहां भी जगह काफी संकरी और निकलने का एक ही रास्ता था। चप्पल बनाने में प्रयुक्त केमिकल की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नही था। इतनी भीषण आग इसी केमिकल के कारण लगी।
मजदूरों की अपनी वर्गीय हैसियत में भी कोई नई बात नही थी। फिलीपीन्स में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी इन्हें आधी मजदूरी ही मिलती थी। लगभग सभी मजदूर ठेका मजदूर थे। और इनमें अधिकांश महिलाएं थी।
वहां का लेबर विभाग, पुलिस और चप्पल बनाने वाली केन्टेक्स कम्पनी के मालिक आपस में मिले हुए थे और मजदूरों के शोषण में इन तीनों की भागीदारी होती थी।
फिलीपीन्स सरकार की प्रतिक्रिया भी कुछ नयी नहीं – ‘दोषियों को बख्शा नही जायेगा’, ‘जांच कमेटी बैठा दी गयी है’, और ‘पुलिस को हाई एलर्ट पर रखा गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।’

अब अपने देश में आते है। मजदूरों के लिए भारत में भी स्थिति इतनी ही खराब है। बस फर्क यह है कि यहां सब कुछ ‘मैक्रो’ स्तर पर नहीं बल्कि ‘माइक्रो’ स्तर पर घटित हो रहा है। इसलिए राना प्लाजा या केन्टेक्स जैसी राष्ट्रीय न्यूज नही बन पाती। बल्कि सचाई बहुत भयावह है। आपको जानकर आश्चर्य होेगा कि भारत में एक दो नही चार चार राना प्लाजा (राना प्लाजा घटना में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।) हर साल घटित हो रहा है। ‘अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं में हर साल 40 हजार से ज्यादा लोग मारे जाते है। हम अनुमान लगा सकते है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा। बहुत सी घटनाएं रिपोर्ट नहीं हो पाती या उन्हे चालाकी से छुपा दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है। कुछ समय पहले एक ‘फैक्ट फाइन्डिंग’ के दौरान ही एक फैक्टरी की चिमनी से एक मजदूर गिर गया। मेन गेट पर जो गार्ड खड़ा था वह दौड़ा और उसने उस घायल मजदूर की जेब से सबसे पहले ‘जाब कार्ड’ निकाला और उसे फाड़ दिया लेकिन तभी दूसरे मजदूर भी आ गये और उस गार्ड को यह काम करते देख लिया और उसकी धुनाई शुरु कर दी। बाद में पता चला कि कम्पनी की तरफ से उस गार्ड को (और उन जैसे अनेकों गार्डो को) हिदायत दी गयी थी कि जब भी कोई मजदूर घायल हो और उसके मरने की संभावना हो तो मौका मिलते ही उसका जाब कार्ड गायब कर दो ताकि सबूत ही ना रहे कि वह इस फैैक्टरी में काम करता था। बाद में पता चला कि चिमनी से गिरे उस घायल मजदूर की मौत हो गयी।
अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की यह रिपोर्ट 2001 की हैं। तबसे स्थितियां और बदतर ही हुई हैं। गौरतलब है कि इन 40 हजार मौतों में वे मौतें शामिल नहीं हैं जो औद्योगिक प्रदूषण जनित बीमारियों से होती है। जैसे ‘सिलकोसिस’ आदि से होने वाली मौतें।
वहीं दुनिया के पैमाने पे बात करें तो यह आंकड़ा और भयावह हो जाता है। उसी श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में औद्योगिक दुर्घटनाओं और उद्योग जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतें प्रति वर्ष करीब 22 लाख हैं।
आज का परिदृश्य यह है कि वैश्विक पूंजी ने वैश्विक श्रम के खिलाफ एक जंग छेड़ा हुआ है। यह जंग ना सिर्फ श्रम यानी मजदूरों के खिलाफ है बल्कि पर्यावरण यानी हमारी इस धरती के भी खिलाफ है क्योकि मुनाफा पैदा करने के लिए उन्हे ना सिर्फ मजदूरों की जरुरत है बल्कि कच्चे माल यानी खनिज सम्पदा की भी जरुरत है।
दुःख इस बात का है कि हमारे ज्यादातर बुद्धिजीवी इस युद्ध पर पर्दा डालने का काम करते हैं। लेकिन यह पर्दा बहुत झीना है और जल्द ही मजदूर वर्ग इस युद्ध को साफ साफ देखने लगेगा। पिछले दिनों दुनिया के अनेक देशों में मजदूरों की जो बड़ी बड़ी हड़तालें और प्रदर्शन हुए हैं वो अनेक मायनों में 60 के दशक की याद दिलाते हैं। यानी बहुत से मजदूर अब इस युद्ध को उसके असली रुप में देखने लगे हैं और अपने आपको उसके हिसाब से तैयार भी करने लगे हैं।

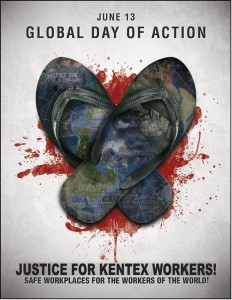
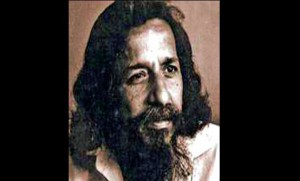
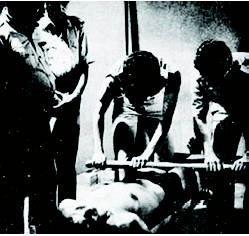

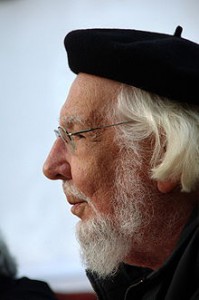

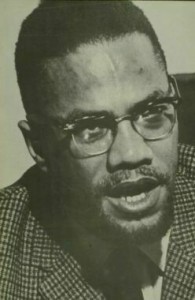
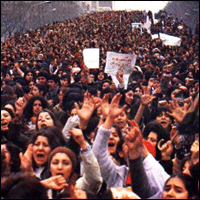
![▶ Shots In The Dark Silence on Vaccine.mp4_snapshot_00.05.57_[2015.03.04_14.01.45]](https://kritisansar.noblogs.org/files/2015/03/▶-Shots-In-The-Dark-Silence-on-Vaccine.mp4_snapshot_00.05.57_2015.03.04_14.01.45-300x172.jpg)