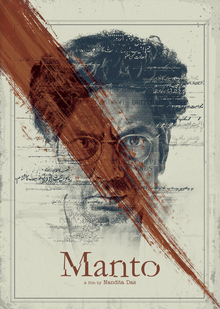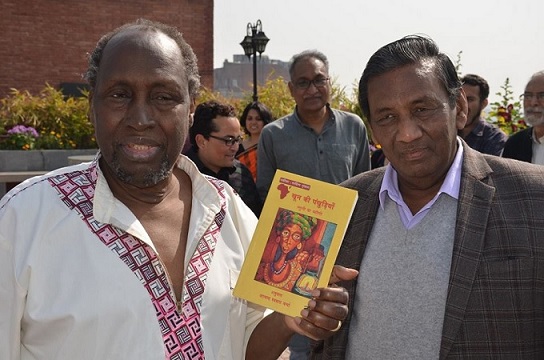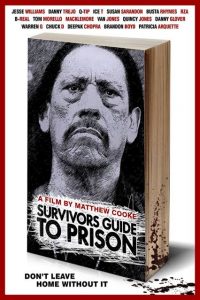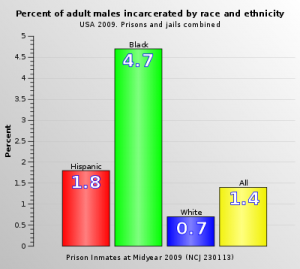सत्ता के खिलाफ मनुष्य का संघर्ष भूल जाने के खिलाफ याद करने का संघर्ष है।
मिलान कुन्देरा
‘कस्तूरी बसु’ और ‘मिताली विस्वास’ द्वारा निर्देशित डाकूमेन्टरी फिल्म ‘एस डी ः सरोज दत्त एण्ड हिज टाइम्स’ वास्तव में भूलने के खिलाफ याद करने का ही संघर्ष है। नक्सलवादी आन्दोलन के प्रमुख हस्ताक्षर ‘सरोज दत्त’ पर केन्द्रित यह फिल्म उनके बहाने उस पूरे दौर को एक तरह से ‘फ्रीज फ्रेम’ करती है जिसे आशा और उम्मीदों का दशक भी कहा जाता है। इस दौर के नौजवान से जब नौकरी के लिए एक इण्टरव्यू में यह सवाल पूछा जाता है कि 60 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है तो वह कहता है – वियतनाम का युद्ध। इण्टरव्यू लेने वाला पैनल चकित होते हुए कहता है कि इसी दशक में तो मानव चाॅद पर भी गया है। क्या यह बड़ी चीज नहीं है तो नौजवान कहता है कि तकनीक और विज्ञान का जिस तरह से विकास हो रहा था, उससे चाॅद पर जाना अपेक्षित था, लेकिन वियतनाम में साधारण लोगों ने जिस असाधारण साहस और त्याग का परिचय दिया है वह अप्रत्याशित था। ‘सत्यजीत रे’ ने अपनी फिल्म ‘प्रतिद्वन्दी‘ में इस मशहूर दृृश्य के बहानेे उस समय के मूड को बखूबी दर्शाया है। नक्सलवादी आन्दोलन उसी कड़ी में साधारण लोगों की असाधारण गाथा है।
फिल्म की शुरूआत सरोज दत्त के रूप मेंं उन्हीं जैसे एक काल्पनिक व्यक्ति के ‘स्लो मोशन’ ब्लैक एण्ड हवाइट इमेज से होती है। भोर का समय है, मैदान में एक व्यक्ति कसरत कर रहा है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और यह काल्पनिक सरोज दत्त स्लो मोशन में ही स्क्रीन से नीचे खिसक जाता है। पहला ही दृृश्य इतना प्रभावकारी है कि फिर आप फिल्म से बंध जाते है। स्क्रीन पर कसरत करता हुआ दूसरा व्यक्ति कौन था। कहीं यह बंगला फिल्म के मशहूर कलाकार ‘उत्तम कुमार’ की ओर संकेत तो नहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सुबह की सैर के वक्त सरोज दत्त को पुलिस द्वारा गोली मारते देखा था। लेकिन उन्होंने अपना मुंह कभी नहीं खोला। बस एक बार एक पार्टी में शराब के नशे में उन्होंने यह बात कबूल की। पर फिल्म मेंं इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं है।
फिल्म की शुरूआत में सरोज दत्त की पत्नी ‘बेला बोस’ का इण्टरव्यू बेहद रोचक है। आश्चर्य होता है कि इस उम्र मेंं भी उनकी यादाश्त इतनी ‘शार्प’ है। ‘पोलिटिकली करेक्ट’ क्या है इसकी पकड़ उन्हें अभी भी है। कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृृत्व द्वारा तेभागा आन्दोलन को वापस लेने और महिला क्रान्तिकारियों को ‘किचन में वापस जाओ‘ कहने को अभी भी बेला बहुत कड़वाहट से याद करती हैं। वे यह भी याद करती हैं कि कैसे सरोज दत्त ने ‘अमृृत बाजार पत्रिका’ में काम करते हुए मलाया के क्रान्तिकारियों को डाकू कहने से इन्कार कर दिया और प्रतिरोध स्वरूप नौकरी छोड़ दी।
बाद में निमाई घोष, कानू सान्याल, कोंकन मजुमदार आदि उनके समकालीन नक्सलवारियों और आज के बुद्धिजीवियों से इण्टरव्यू के बहाने उनके राजनीतिक जीवन, उनके लेखन और उस दौर के घटनाक्रम पर बखूबी प्रकाश पड़ता है। यहां नक्सलवादी आन्दोलन की मुख्य कड़ी भूमिहीन किसान और उनके विद्रोह को एक परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश की गयी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस आन्दोलन से प्रभावित ज्यादातर फिल्में शहरी नौजवानों की आशाओं आकांक्षाओंं के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। इसी अर्थ में चारू मजुमदार के बेटे अभिजीत मजुमदार द्वारा लिया गया आदिवासी महिला ‘मुण्डा‘ का इण्टरव्यू बहुत महत्वपूर्ण है।
फिल्म मेंं सरोज दत्त की उस समय के मशहूर बुद्धिजीवी व फ्रन्टियर के संस्थापक संपादक ‘समर सेन’ के साथ मशहूर बहस का भी जिक्र है जिसकी अनुगंूज आज भी सुनाई देती है। हालांकि इस विषय को बिल्कुल भी खोला नहीं गया है। इस बहस को थोड़ा खोलने से फिल्म को एक नया आयाम मिलता क्योकि यह बहस इन दोनों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि अन्तर्रा’ट्रीय स्तर पर इसमें लूकाज-ब्रेख्त-अन्र्सट फिशर-ज्यादानोव जैसे लोग शामिल थे। बंाग्ला साहित्य में आज भी यह बहस घूम फिर कर सामने आ खड़ी होती है। सुशीतल राय चौधरी के साथ मूर्ति भंजन पर सरोज दत्त की बहस को जरूर थोड़ी जगह मिली है। ‘ईश्वरचन्द्र विद्यासागर’ की मूर्ति उस समय नक्सलवादियों द्वारा तोड़ी गयी थी और दुबारा आज यह भाजपाईयोंं द्वारा तोड़ी गयी। प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाता है कि पिछले 50 सालों में कुल मिलाकर राजनीति कैसे वाम से दक्षिण की ओर शिफ्ट हुई है। और यह सिर्फ भारत के पैमाने पर नहीं वरन्् विश्व के पैमाने पर घटित हुआ है या हो रहा है।
फिल्म में ‘देवीप्रसाद चट््टोपाध्याय’ और ‘मंजूषा चट््टोपाध्याय’ जिस तरह से सरोज दत्त को याद करते हैं, उससे उनके व्यक्तित्व का एक और विराट दरवाजा खुल जाता है। आज 50 साल बाद भी मंजूषा सरोज दत्त को याद करते हुए रो पड़ती हैं मानो कल की ही कोई घटना बयां कर रही हों।
सरोज दत्त और उनके समकालीन क्रान्तिकारी ना सिर्फ नक्सलवादी आन्दोलन की पैदाइश थे, बल्कि उस समय के विश्व क्रान्तिकारी आन्दोलन की भी पैदाइश थे। इसे एक दृृश्य में बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है, जहां सरोज दत्त का कल्पनिक चरित्र ट्रेन या ट्राम में बैठा है और उसकी पृृष्ठभूमि मेंं विश्व के तमाम आन्दोलनों की छवियां (आर्काइवल फुटेज) एक दूसरे मेंं घुल मिल रही हैं। इसी क्रम में ‘पैट्रिक लुमुम्बा’ की अन्तिम दिनो की ‘न्यूज रील’ ‘राउल पेक’ की मशहूर फिल्म ‘लुमुम्बा‘ की याद ताजा कर देती है। ‘न्यूज रील’ और ‘सिनेमा रील’ आपस में घुल मिल जाते है। यथार्थ फिक्शन हो जाता है और फिक्शन यथार्थ हो जाता है।
फिल्म में सरोज दत्त की कविताओं और उनके अनुवादों का जिस कौशल के साथ सतत इस्तेमाल किया गया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाये कम है। फिल्म में अनेक उप विषयोंं को ध्यान में रखते हुए सरोज दत्त की कविताओं की मूल पांडूलिपि की तस्वीरों की पृृष्ठभूमि में जिस तरह उनकी कविताएं स्क्रीन पर लगातार तैरती है, वह बेहद शानदार अनुभव है। यहां ना सिर्फ उनकी कविताओंं का गहरा आस्वाद मिलता है वरन इन कविताओं से उस वक्त चर्चा किये जाने वाले विषयोंं को भी एक गहराई मिल जाती है।
फिल्म अपने करीब 2 घण्टे के इस ‘लांग मार्च’ मेंं कई खूबसूरत जनवादी गीतों का इस्तेमाल करती है। इससे उस समय का मूड ताजा हो जाता है। गौतम घोष की ‘मां भूमि‘ की क्लिपिंग मेंं नौजवान ‘गदर’ को देखना काफी सुखद है। इसी तरह ‘मृृणाल सेन’ और ‘एस सुखदेव’ की फिल्मों की क्लिपिंग्स का बहुत प्रासंगिक व सुन्दर इस्तेमाल किया गया है। बंगाल की सड़कों पर नौजवानों के संघर्ष की ‘आर्काइवल इमेज’ पैट्रीसियों गुजमान की मशहूर फिल्म ‘बैटल आॅफ चिली‘ की याद दिलाते हैं।
फिल्म में दोनों डायरेक्टरों ने जिस तरह आत्म विश्वास और बेहद इत्मीनान से खुद भी स्क्रीन साझा किया है उससे ऐसा अहसास होता है कि हम भी उस दौर के इतिहास की उनकी इस खोज मेंं शामिल हैं। यानी उनके साथ हम भी ‘इतिहास के सिपाही’ है।
फिल्म मेंं ‘वर्तमान सेटिंग’ में अनेक जगहों पर ‘सीपीआई एम एल’ के झण्डे लहराते दिखाये गये है। इसके अलावा इसी पार्टी के सीसी सदस्यों द्वारा सरोज दत्त को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया गया है। आज का सीपीआई एम एल (लिबरेशन) सरोज दत्त के जमाने का सीपीआई एम एल नहीं है। इन दृृश्योंं से चाहे-अनचाहे कहीं ना कहीं उस दौर के व सरोज दत्त के विशाल व्यक्तित्व को सीमित करने का प्रयास झलकता है। इससे बचा जा सकता था।
इसके अलावा जिस वक्तव्य से फिल्म का समापन किया गया है वह कतई विषय की उदात्तता और उसमें निहित ‘क्रान्तिकारी आशावाद’ से मेल नहीं खाता। 1967 का नक्सलवादी आन्दोलन उस वक्त के सवालों के तमाम जवाबों के कनफ्यूजन से उस समय की पीढ़ी को निकालने का भी आन्दोलन था और आज हमें फिर यह कहना पड़ रहा है कि सवालोंं के कई उत्तर हो सकते हैं? क्या हम पुनः 1967 के पहले वाली स्थिति में पहंुच गये हैं? फिर नक्सलवादी आन्दोलन का सबक क्या है? सरोज दत्त की विरासत क्या है? वह विरासत आज किनके पास है। आज का संकट क्या है? इन सबके कई जवाब नहीं वरन एक ही जवाब है और वह फिल्म के विषय और सरोज दत्त की कविताओं में है। अच्छा होता यदि फिल्म का समापन सरोज दत्त की कविताओं या उनके जैसे किसी क्रान्तिकारी के वक्तव्य से किया जाता।
मार्क्स ने ‘पेरिस कम्यून’ की समीक्षा करते हुए अन्त में इसका इस तरह समापन किया है- ”यह संघर्ष अपने अनेक विकसित आयामों में बार बार उठ खड़ा होगा और इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में कौन विजयी होगा -शोषण करने वाले कुछ लोग या कामगारों का विशाल बहुमत”।
बहरहाल कुल मिलाकर यह एक जरूरी और कई बार देखी जाने वाली फिल्म है।
-
Recent Posts
Recent Comments
- shachinder on Geoengineering, Genetic engineering and Weather warfare
- एंजेलिना जोली की बहादुरी का सच: जनसत्ता में 'कृत on एंजेलिना जोली की ‘बहादुरी’ का सच……….
- फसल के गीत: जनसत्ता में 'कृति मेरे मन की' - Blogs In Media on फसल के गीत
- sonesh on Coal Curse: A film on the political economy of coal in India
- Williamfoer on Quantum physics, dialectics and society: from Marx and Engels to Khrennikov and Haven by Ben Gliniecki
Archives
- February 2026
- April 2025
- May 2024
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- June 2019
- May 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- December 2017
- November 2017
- September 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- August 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- December 2015
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- August 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
हमारे दोस्त.....
- Asia Monitor Resource Centre
- China Labour Net
- CorpWatch
- Encyclopedia of Philosophy
- etcgroup
- Film Theory and Philosophy
- Frontierweekly
- Global Research
- Ground Reality
- International Journal
- macroscan
- muslimmirror.com
- net security
- On Recession
- Original People
- progressive poetry
- Radical Anthropology
- rupeindia
- scroll
- South Asia Citizens Web
- The Case for Global Film
- The Wire
- Thescientificworldview
- Top Documentary Films
- world socialist web site
- अनुवाद,हिन्दी और भाषाओं की दुनिया
- इप्टानामा
- कविता कोश
- चार्वाक
- जन जवार
- जनपक्ष
- जनपथ
- प्रतिभास
- प्रतिरोध. काॅम
- भारत का इतिहास
- मुक्तिबोध
- साहित्य समय
- हस्तक्षेप
- हाशिया
Meta